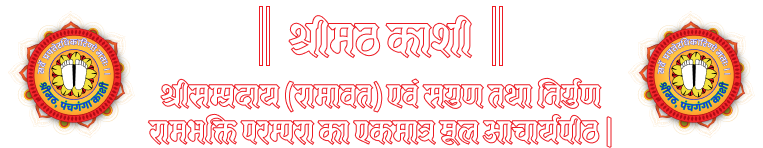जगतगुरु रामानंदाचार्य अपने द्वादश शिष्यों के साथ
स्वामी रामानंद़ को मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। उन्होंने रामभक्ति की धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया.वे पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। उनके बारे में प्रचलित कहावत है कि -द्वविड़ भक्ति उपजौ-लायो रामानंद.यानि उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। उन्होंने तत्कालीन समाज में ब्याप्त कुरीतियों जैसे छूयाछूत, ऊंच-नीच और जात-पात का विरोध किया .
आरंभिक जीवन
स्वामी रामानंद का जन्म प्रयाग(इलाहाबाद) में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम सुशीला देवी और पिता का नाम पुण्य सदन शर्मा था। आरंभिक काल में हीं उन्होंने कई तरह के अलौकिक चमत्कार दिखाने शुरू किये.धार्मिक विचारों वाले उनके माता-पिता ने बालक रामानंद को शिक्षा पाने के लिए काशी के स्वामी राधवानंद के पास श्रीमठ भेज दिया. श्रीमठ में रहते हुए उन्होंने वेद, पुराणों और दूसरे धर्मग्रंथों का अध्ययन किया और प्रकांड विद्वान बन गये।पंचगंगा घाट स्थित श्रीमठ में रहते हुए उन्होंने कठोर साधना की .उनके जन्म दिन को लेकर कई तरह की भ्रंतियां प्रचलित है लेकिन अधिकांश विद्वान मानते हैं कि स्वामीजी का जन्म 1400 ईस्वी में हुआ था। यानि आज से कोई सात सौ दस साल पहले.
शिष्य परंपरा
स्वामी रामानंद ने राम भक्ति का द्वार सबके लिए सुलभ कर दिया. उन्होंने अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, नाभा दास, नरहर्यानंद, सुखानंद, कबीर, रैदास, सुरसरी, पदमावती जैसे बारह लोगों को अपना प्रमुख शिष्य बनाया, जिन्हे द्वादश महाभागवत के नाम से जाना जाता है। इनमें कबीर दास और रैदास आगे चलकर काफी ख्याति अर्जित किये. कबीर औऱ रविदास ने निर्गुण राम की उपासना की.इस तरह कहें तो स्वामी रामानंद ऐसे महान संत थे जिसकी छाया तले सगुण और निर्गुण दोनों तरह के संत-उपासक विश्राम पाते थे। जब समाज में चारो ओर आपसी कटूता और वैमनस्य का भाव भरा ङुआ था, वैसे समय में स्वामी रामानंद ने नारा दिया-जात-पात पूछे ना कोई-ङरि को भजै सो हरी का होई. उन्होंने सर्वे प्रपत्तेधिकारिणों मताः का शंखनाद किया और भक्ति का मार्घ सबके लिए खोल दिया. उन्होंने महिलाओं को भी भक्ति के वितान में समान स्थान दिया. उनके द्वारा स्थापित रामानंद सम्प्रदाय या रामावत संप्रदाय आज वैष्णवों का सबसे बड़ा धार्मिक जमात है। वैष्णवों के 52 द्वारों में 36 द्वारे केवल रामानंदियों के हैं। इस संप्रदाय के संत बैरागी भी कहे जाते हैं। इनके अपने अखाड़े भी हैं। यूं तो रामानंद सम्प्रदाय की शाखाएं औऱ उपशाखाएँ देश भर में फैली हैं। लेकिन अयोध्या,चित्रकूट,नाशिक, हरिद्वार में इस संप्रदाय के सैकड़ो मठ-मंदिर हैं। काशी के पंचगंगा घाट पर अवस्थित श्रीमठ, दुनिया भर में फैले रामानंदियों का मूल गुरुस्थान है। दूसरे शब्दों में कहें तो काशी का श्रीमठ हीं सगुण और निर्गुण रामभक्ति परम्परा और रामानंद सम्प्रदाय का मूल आचार्यपीठ है। वर्तमान में जगदगुरू रामानंदाचार्य स्वामी श्रीरामनरेशाचार्यजी महाराज, श्रीमठ के गादी पर विराजमान हैं। वे न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं और संत समाज में समादृत हैं।
भक्ति-यात्रा
स्वामी रामानंद ने भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए देश भर की यात्राएं की.वे पुरी औऱ दक्षिण भारत के कई धर्मस्थानों पर गये और रामभक्ति का प्रचार किया। पहले उन्हें स्वामी रामनुज का अनुयाय़ी माना जाता था लेकिन श्रीसम्प्रदाय का आचार्य होने के बावजूद उन्होंने अपनी उपासना पद्धति में ऱाम और सीता को वरीयता दी. उन्हें हीं अपना उपास्य बनाया.राम भक्ति की पावन धारा को हिमालय की पावन ऊंचाईयों से उतारकर स्वामी रामानंद ने गरीबों और वंचितों की झोपड़ी तक पहुंचाया. वे भक्ति मार्ग के ऐसे सोपान थे जिन्होंने वैष्णव भक्ति साधना को नया आयाम दिया.उनकी पवित्र चरण पादुकायें आज भी श्रीमठ, काशी में सुरक्षित हैं, जो करोड़ों रामानंदियों की आस्था का केन्द्र है। स्वामीजी ने भक्ति के प्रचार में संस्कृत की जगह लोकभाषा को प्राथमिकता गी.उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की जिसमें आनंद भाष्य पर टीका भी शामिल है।वैष्णवमताब्ज भाष्कर भी उनकी प्रमुख रचना है।
चिंतनधारा
भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य और संस्कृति के विकास में भागवत धर्म तथा वैष्णव भक्ति से संबद्ध वैचारिक क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैष्णव भक्ति के महान संतों की उसी श्रेष्ठ परंपरा में आज से लगभग सात सौ नौ वर्ष पूर्व स्वामी रामानंद का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने श्री सीताजी द्वारा पृथ्वी पर प्रवर्तित विशिष्टाद्वैत (राममय जगत की भावधारा) सिद्धांत तथा रामभक्ति की धारा को मध्यकाल में अनुपम तीव्रता प्रदान की. उन्हें उत्तरभारत में आधुनिक भक्ति मार्ग का प्रचार करने वाला और वैष्णव साधना के मूल प्रवर्त्तक के रूप में स्वीकार किया जाता है। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति के अनुसार-
भक्ति द्रविड़ ऊपजी, लायो रामानंद.
रामानंद का समन्वयवाद
तत्कालीन समाज में विभिन्न मत-पंथ संप्रदायों में घोर वैमनस्यता और कटुता को दूर कर हिंदू समाज को एक सूत्रबद्धता का महनीय कार्य किया। स्वामीजी ने मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम को आदर्श मानकर सरल रामभक्ति मार्ग का निदर्शन किया। उनकी शिष्य मंडली में जहां एक ओर कबीरदास, रैदास, सेननाई और पीपानरेश जैसे जाति-पाति, छुआछूत, वैदिक कर्मकांड, मूर्तिपूजा के विरोधी निर्गुणवादी संत थे तो दूसरे पक्ष में अवतारवाद के पूर्ण समर्थक अर्चावतार मानकर मूर्तिपूजा करने वाले स्वामी अनंतानंद, भावानंद, सुरसुरानंद, नरहर्यानंद जैसे सगुणोपासक आचार्य भक्त भी थे। उसी परंपरा में कृष्णदत्त पयोहारी जैसा तेजस्वी साधक और गोस्वामी तुलसीदास जैसा विश्व विश्रुत महाकवि भी उत्पन्न हुआ। आचार्य रामानंद के बारे में प्रसिद्ध है कि तारक राममंत्र का उपदेश उन्होंने पेड़ पर चढ़कर दिया था ताकि सब जाति के लोगों के कान में पड़े और अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके. उन्होंने नारा दिया था-
जाति-पाति पूछे न कोई.
हरि को भजै सो हरि का होई.
आचार्यपाद ने स्वतंत्र रूप से श्रीसंप्रदाय का प्रवर्तन किया। इस संप्रदाय को रामानंदी अथवा वैरागी संप्रदाय भी कहते हैं। उन्होंने बिखरते और नीचे गिरते हुए समाज को मजबूत बनाने की भावना से भक्ति मार्ग में जाति-पांति के भेद को व्यर्थ बताया और कहा कि भगवान की शरणागति का मार्ग सबके लिए समान रूप से खुला है-
सर्व प्रपत्तिधरकारिणो मता:
कहकर उन्होंने किसी भी जाति-वरण के व्यक्ति को राममंत्र देने में संकोच नहीं किया। चर्मकार जाति में जन्मे रैदास और जुलाहे के घर पले-बढ़े कबीरदास इसके अनुपम उदाहरण हैं।
धार्मिक अवदान
मध्ययुगीन धर्म साधना के केंद्र में स्वामी जी की स्थिति चतुष्पथ के दीप-स्तंभ जैसी है। उन्होंने अभूतपूर्व सामाजिक क्रांति का श्रीगणेश करके बड़ी जीवटता से समाज और संस्कृति की रक्षा की. उन्हीं के चलते उत्तरभारत में तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा और वहां सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना संभव हो सकी. उस युग की परिस्थितियों के अनुसार, वैरागिनी साधु समाज को अस्त्र-शस्र से सज्जित अनी के रूप में संगठित कर तीर्थ-व्रत की रक्षा के लिए, धर्म का सक्रिय मूर्तिमान स्वरूप खड़ा किया। तीर्थस्थानों से लेकर गांव-गांव में वैरागी साधुओं ने अखाड़े स्थापित किए. मूल्य ह्रास की इस विषम अवस्था में भी संपूर्ण संसार में रामानंद संप्रदाय के सर्वाधित मठ, संत, रामगुणगान, अखंड रामनाथ संकीर्तन आज भी व्यवस्थित हैं और सर्वत्र आध्यामिक आलोक प्रसारित कर रहे हैं। वैष्णवों के बावन द्वारों में सर्वाधिक सैंतीस द्वारे इसी संप्रदाय से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त भी फैली इसकी शाखा, प्रशाखा और अवान्तर शाखाएं जैसे- रामस्नेही, कबीरदासी, घीसापंथी, दादूपंथ आदि नामों से इस संप्रदाय की मूलभावना की संवाहिका बनी हैं। यह स्वामी रामानंद के ही व्यक्तित्व का प्रभाव था कि हिंदू-मुस्लिम वैमनस्य, शैव-वैष्णव विवाद, वर्ण-विद्वेष, मत-मतांतर का झगड़ा और परस्पर सामाजिक कटुता बहुत हद तक कम हो गई। उनके ही यौगिक शक्ति के चमत्कार से प्रभावित होकर तत्कालीन मुगल शासक मोहम्मद तुगलक संत कबीरदास के माध्यम से स्वामी रामानंदाचार्य की शरण में आया और हिंदुओं पर लगे समस्त प्रतिबंध और जजियाकर को हटाने का निर्देश जारी किया। बलपूर्वक इस्लाम धर्म में दीक्षित हिंदुओं को फिर से हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए परावर्तन संस्कार का महान कार्य सर्वप्रथम स्वामी रामानंदाचार्च ने ही प्रारंभ किया। इतिहास साक्षी है कि अयोध्या के राजा हरिसिंह के नेतृत्व में चौंतीस हजार राजपूतों को एक ही मंच से स्वामीजी ने स्वधर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। ऐसे महान संत, परम विचारक, समन्वयी महात्मा का प्रादुर्भाव तीर्थराज प्रयाग में एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्मतिथि को लेकर मतभेद होने के बावजूद रामानंद संप्रदाय में मान्यता है कि आद्य जगद्गुरू का प्राकट्य माघ कृष्ण सप्तमी संवत् 1356 को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित पुण्य सदन शर्मा और माता का नाम सुशीला देवी था। धार्मिक संस्कारों से संपन्न पिता ने रामानंद को काशी के श्रीमठ में गुरू राघवानंद के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण के लिए भेजा. कुशाग्रबुद्धि के रामानंद ने अल्पकाल में ही सभी शास्त्रों, पुराणों का अध्ययन कर प्रवीणता प्राप्त कर ली. गुरू राघवानंद और माता-पिता के दबाव के बावजूद उन्होंने गृहस्थाश्रम स्वीकार नहीं किया और आजीवन विरक्त रहने का संकल्प लिया। ऐसे में स्वामी रामानंद को रामतारक मंत्र की दीक्षा प्रदान की. रामानंद ने श्रीमठ की गुह्य साधनास्थली में प्रविष्ट हो राममंत्र का अनुष्ठान तथा अन्यान्य तांत्रिक साधनाओं का प्रयोग करते हुए घोर तपश्चर्या की. योगमार्च की तमाम गुत्थियों को सुलझाते हुए उन्होंने अष्टांग योग की साधना पूर्ण की. दीर्घायुष्य प्राप्त करने के कारण जगद्गुरू राघवानंद ने अपने तेजस्वी और प्रिय शिष्ट रामानंद को श्रीमठ पीठ की पावन पीठ पर अभिषिक्त कर दिया. अपने पहले संबोधन में ही जगदगुरू रामानंदाचार्य ने हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को दूर करने तथा परस्पर आत्मीयता एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार के बदौलत धर्म रक्षार्थ विराट संगठित शक्ति खड़ा करने के संकल्प व्यक्त किया। काशी के परम पावन पंचगंगा घाट पर अवस्थित श्रीमठ, आचार्यपाद के द्वारा प्रवाहित श्रीराम प्रपत्ति की पावनधारा के मुख्यकेंद्र के रूप में प्रतिष्ठित होकर उसी ओजस्वी परंपरा का अनवरत प्रवर्तन कर रहा है। आज भी श्रीमठ आचार्यचरण की परिकल्पना के अनुरूप उनके द्वारा प्रज्ज्वलित दीप से जनमानस को आलोकित कर रहा है। यही वह दिव्यस्थल है, जहां विराजमान होकर स्वामीजी ने अपने परमप्रतापी शिष्यों के माध्यम से अपनी अनुग्रहशक्ति का उपयोग किया था। रामानंदाचार्च पीठ का पवित्र केंद्र सारे देश में फैले रामानंद संप्रदाय का मुख्यालय है। श्रीमठ में अवस्थित रामानंदाचार्च की चरणपादुका दुनियाभर में बिखरे रामानंदी संतों, तपस्वियों एवं अनुयायियों की श्रद्धा का अन्यतम बिंदु है। यह परम सौभाग्य और संतोष का विषय है कि श्रीमठ के वर्तमान पीठासीन आचार्य स्वामी रामनरेशाचार्यजी भी स्वामी रामानंदाचार्च की प्रतिमूर्ति जान पड़ते हैं। उनकी कल्पनाएं, उनका ज्ञान, उनकी वग्मिता और सबसे अच्छी उनकी उदारता और संयोजन चेतना ऐसी है कि यह विश्वास किया जाता है कि स्वामी रामानंद का व्यक्तित्व कैसा रहा होगा. वर्तमान जगद्गुरू रामानंदाचार्च पद प्रतिष्ठित स्वामी रामनरेशाचार्य जी महाराज के सत्प्रयासों का नतीजा है कि श्रीमठ से कभी अलग हो चुकी कबीरदासीय, रविदासीय, रामस्नेही, प्रभृति परंपराएं वैष्णव के सूत्र में बंधकर श्रीमठ से एकरूपता स्थापित कर रही है। कई परंपरावादी मठ मंदिरों की इकाईयां श्रीमठ में विलीन हो रही हैं। तीर्थराज प्रयाग के दारागंज स्थित आद्य जगद्गुरू रामनंदाचार्य का प्राकट्यधाम भी इनकी प्रेरणा से फिर भव्य स्वरूप में प्रकट हुआ है। स्वामी रामानंद को रामोपासना के इतिहास में एक युगप्रवर्तक आचार्य माना जाता है। उन्होंने श्रीसंप्रदाय के विशिष्टाद्वैत दर्शन और प्रपतिसिद्धांत को आधार बनाकर रामावत संप्रदाय का संगठन किया। श्रीवैष्णवों के नारायण मंत्र के स्थान पर रामतारक अथवा षडक्षर राममंत्र को सांप्रदायिक दीक्षा का बीजमंत्र माना. बाह्य सदाचार की अपेक्षा साधना में आंतरिक भाव की शुद्धता पर जोर दिया, छुआछूत, ऊंच-नीच का भाव मिटाकर वैष्णव मात्र में समता का समर्थन किया। नवधा से परा और प्रेमासक्ति को श्रेयकर बताया. साथ-साथ सिद्धांतों के प्रचार में परंपरापोषित संस्कृत भाषा की अपेक्षा हिंदी अथवा जनभाषा को प्रधानता दी. स्वामी रामानंद ने प्रस्थानत्रयी पर विशिष्टाद्वैत सिद्धांतनुगुण स्वतंत्र आनंद भाष्य की रचना की. तत्व एवं आचारबोध की दृष्टि से वैष्णवमताब्ज भास्कर, श्रीरामपटल, श्रीरामार्चनापद्धति, श्रीरामरक्षास्त्रोतम जैसी अनेक कालजयी मौलिक ग्रंथों की रचना की. स्वामी रामानंद के द्वारा दी गई देश-धर्म के प्रति इन अमूल्य सेवाओं ने सभी संप्रदायों के वैष्णवों के हृदय में उनका महत्व स्थापित कर दिया. भारत के सांप्रदायिक इतिहास में परस्पर विरोधी सिद्धांतों तथा साधना-पद्धतियों के अनुयायियों के बीच इतनी लोकप्रियता उनके पूर्व किसी संप्रदाय प्रवर्तक को प्राप्त न हो सकी. महाराष्ट्र के नाथपंथियों ने ज्ञानदेव के पिता विट्ठल पंत के गुरू के रूप में उन्हें पूजा, अद्वैत मतावलंबियों ने ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी के रूप में उन्हें अपनाया. बाबरीपंथ के संतों ने अपने संप्रदाय के प्रवर्तक मानकर उनकी वंदना की और कबीर के गुरू तो वे थे ही, इसलिे कबीरपंथियों में उनका आदर स्वाभाविक है। स्वामी-रामानंद के व्यक्तित्व की इस व्यपाकता का रहस्य, उनकी उदार एवं सारग्राही प्रवृति और समन्वयकारी विचारधारा में निहित है। निश्चय हीं उनके विराट व्यक्तित्व एवं व्यापक महत्ता के अनुरूप कतिपय आर्षग्रंथ एवं संत-साहित्य में उल्लेखित उनके रामावतार होने का वर्णन अक्षरश: प्रमाणित होता है। रामनंद: स्वयं राम: प्रादुर्भूतो महीतले।
श्रीमठ दर्शन
यह हजारा है, हजार दीपों का स्टैंड. इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने १८वी सदी में काशी विश्वनाथ मंदिर और श्रीमठ का जीर्णोधार करवाया था, तभी यह हजारा बना. इसके बगल में एक छोटा हजारा भी है. देव दीपावली को इसे रौशन किया जाता है, तब देखने के लिए बनारस भर के लोग जुटते हैं और गंगा की रौनक देखने लायक हो जाती है. हजारा के लिए आइना बन जाती है गंगा मैया.
श्रीमठ दर्शन
श्रीमठ की तीसरी मंजिल पर विराजमान पावन चरण पादुका और जगदगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज
श्रीमठ के ठीक सामने का घाट और श्रीमठ की बोट(सबसे बड़ी वाली), बनारस की गलियों में जब भीड़ रहती है, तब महाराज जगदगुरु इसी बोट के सहारे दूसरी घाट पर जाकर वहां किसी सड़क वाहन में विराजते हैं. श्रीमठ तक किसी सड़क वाहन के जाने की सुविधा नहीं है. श्रीमठ से करीब एक सवा किलोमीटर दूर वाहन छोड़ देना पड़ता है, और फिर गलियों से होते हुए करीब दस- बारह जगह मुड़ने के बाद गंगा और श्रीमठ के दर्शन होते हैं. जब गलियों में ज्यादा भीड़ नहीं होती और जगदगुरु के पास पूरा समय होता है तो वे भी गलियों से होते हुए लोगों को दर्शन देते हुए निकलते हैं.
श्रीमठ : कल और आज
गंगा मैया की गोद में कुछ आगे बढक़र गहरे तक रचा-बसा श्रीमठ, मानो मां की गोद में अधिकार भाव से विराजमान कोई दुलारी संतान। श्रीमठ की पांचवीं मंजिल पर बालकनी में खड़े होकर जब आगे-पीछे देखता हूं, तो लगता है, बनारस ने श्रीमठ को आगे खड़ा कर दिया है कि तुम आगे रहो, ताकि हम पीछे सुरक्षित रहें। श्रीमठ को देखकर अनायास यह अनुभूति होती है और समझ में आता है कि आखिर क्या होता है, बची हुई थोड़ी-सी जगह में खुद को बचाए रखना। श्रीमठ की यह बची हुई जगह आकार में अत्यंत छोटी है, लेकिन अपने अंतस में अनंतता और अपनी भाव गुरुता को संजोए हुए, प्रेम से सराबोर, भक्ति के अनहद नाद से गुंजायमान। संसार के अत्यंत कठिन व छलिया समय में क्या होता है सन्तत्व, यह केवल श्रीमठ को देखकर ही अनुभूत किया जा सकता है। यहाँ आकर जो अनुभूतियाँ होती हैं, वो दुर्लभ हैं और निस्संदेह, इन अनुभवों का सम्पूर्ण अनुवाद असंभव है।बताते हैं जब गंगा जी का संसार में अवतरण नहीं हुआ था तब भी यह भूमि पावन थी. इस जगह को कभी श्री विष्णु ने अपना स्थाई निवास बनाया था. ग्रंथों में इस स्थान का उल्लेख धर्मनद नाम से भी हुआ है. इस तीर्थ को सतयुग में धर्मनद, त्रेता में धूतपापक, द्वापर में विन्दुतीर्थ एवं कलियुग में पंचनद नाम से जाना गया। धर्मनद तीर्थ तब भी था, जब गंगा जी नहीं थीं। धर्मनद तीर्थ पर दो पवित्र जल धाराएं मिलती थीं – धूतपापा और किरणा। यह संगम स्थल तब भी बहुत पुण्यकारी था। बाद में जब गंगा जी आईं, तो उनके साथ यमुना और सरस्वती भी थीं। बनारस की दो पावन धाराओं का मिलन तीन नई पावन धाराओं से हुआ और इस तरह से धर्मनद तीर्थ पंचनद तीर्थ कहलाने लगा। पंचनद को ही लोगों ने बाद में पंचगंगा कर दिया, भगवान विष्णु द्वारा पवित्र किये गए इसी पंचगंगा घाट पर अनेक वैष्णव संतों ने निवास किया, जगदगुरु रामानन्द जी, श्री वल्लभाचार्य जी, संत एकनाथ, समर्थगुरु रामदास, महात्मा तैलंगस्वामी इत्यादि ने यहीं डेरा डाला. गंगा जी के आने के बाद बनारस में घाट तो खूब बन गए, ज्यादातर घाटों का विकास राजाओं ने करवाया, किन्तु संतों की कृपा व प्रेरणा से जो घाट बना, वह तो केवल पंचगंगा है. ग्रंथों में यह भी आया है कि इस घाट पर स्नान सर्वाधिक पुण्यकारी है. जो लोग इस तथ्य को जानते हैं, वे यहां स्नान व सीताराम दर्शन के लिए अवश्य आते हैं। उर्जा से भरपूर कबीर को यहीं आसरा मिला, यहीं आकर गुरु की खोज पूरी हुई. पंचगंगा घाट की सीढिय़ों पर ही किसी रात लेट गए थे कबीर, और जगदगुरु रामानन्द जी सुबह-सुबह घाट की सीढियां उतर रहे थे, उनके पाँव कबीर पर पड़ गए थे, कबीर भी यही चाहते थे, जगदगुरु रामानन्द जी ने उन्हें हाथों से पकडक़र उठा लिया था, कष्ट मिटाते हुए कहा था, बच्चा राम राम कहो, तुम्हारा कल्याण होगा. उसके बाद पूरे बनारस को पता चल गया कि एक निम्न जाति के कबीर को जगदगुरु रामानन्द जी ने अपना शिष्य बना लिया है. कबीर से जुडी इसके बाद की भी रोचक कथा है, जिसे आप सब जानते हैं.
पंचगंगा घाट श्रीमठ आकर रोम हर्षित हो उठते हैं, बिल्कुल यहीं रहते होंगे आचार्य जगदगुरु श्री रामानन्द जी। यहां कभी विराजती होंगी – कबीर, रैदास, पीपा, धन्ना, सेन और गोस्वामी तुलसीदास जैसी अतुलनीय विभूतियां। यहां पत्थरों के स्पर्श में भी जादू-सा है। जहां आप पांव भी रखते हैं, तो लगता है, ओह, जरा प्रेम से रखा जाए। पंचगंगा घाट के पत्थर इतिहास नहीं बताते, लेकिन यह अनुभूति अवश्य करा देते हैं कि देखो, आए हो, तो जरा ध्यान से, जरा प्यार से, भाव विभोर हो, जरा याद तो करो कि यहां क्या-क्या हुआ होगा। यहां लाखों वैष्णवों, रामानन्दियों ने खरबों बार जपा होगा – सीताराम-सीताराम। यह भूमि पवित्र हो गई, तभी तो बची हुई है।
पंचगंगा घाट बनारस के प्राचीनतम पक्के घाटों में शामिल है। 16 वीं सदी में यहां जयपुर-आमेर के राजा मानसिंह ने भी घाट का निर्माण करवाया था। 18वीं सदी में जीर्णोद्धार का कुछ काम महारानी अहिल्याबाई ने भी करवाया। पहले श्रीमठ काफी विस्तृत था, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि यवनों ने इसे लगभग पूरी तरह से तोड़ दिया। यहां विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुख और रोष होता है, श्रीमठ की जगह यवनों ने अपना विशाल धर्मस्थल बना लिया, जो आज भी श्रीमठ के पीछे स्थित है। यह आक्रमण इस बात का प्रमाण है कि श्रीमठ का भारतीय संस्कृति में कैसा उच्चतम स्थान रहा होगा कि जिसे ध्वस्त करके ही शत्रु आगे बढ़ सकते थे। बनारस में गंगा घाट क्षेत्र में ऐसा विनाशकारी अधार्मिक अतिक्रमण और कहीं नहीं दिखता। उस पावन स्थली को ध्वस्त किया गया, उस महान तीर्थ को ध्वस्त किया गया, जहां से कभी भारतीय संस्कृति को सशक्त करने वाला महान नारा गूंजा था कि जाति-पांति पूछे नहि कोई, हरि को भजे सो हरि का होई।
रामजी की कृपा से पूजनीय है यह धर्मस्थल, जहां ब्राह्मणवाद सम्पूर्ण समाज को समर्पित हो जाता है, जहां चर्मकार रैदास के लिए भी जगह है, तो जाट किसान धन्ना के लिए भी, जहां कबीर जुलाहे को सिर आंखों पर बिठाया जाता है, जहां जात से नाई सेन भी पूजे जाते हैं और जहां राजपूत राजा पीपा को भी सन्त बना दिया जाता है। जहां वर्णभेद नहीं, लिंगभेद नहीं, वर्गभेद नहीं। जहां भगवान के द्वार सबके लिए खुले हैं, जहां पहुंचकर पद्मावती और सुरसरी सन्त हो गईं। ऐसा श्रीमठ हमले का शिकार हुआ, तो उसके पीछे का षडयंत्र प्रत्येक भारतीय को पता होना चाहिए।
आक्रमण व विध्वंस के उपरांत कभी बस आचार्य रामानन्द जी की पादुकाओं का स्थान ही शेष रह गया था, फिर कभी दो मंजिल की एक छोटी-सी इमारत बनी, लेकिन अब थोड़ी-सी जगह में पांच मंजिली इमारत खड़ी है, भीतर-बाहर से पवित्र, प्रेरक, उज्ज्वल। विनाश व विध्वंस के अनगिनत प्रयासों के बावजूद श्रीमठ आज हमारे समय का एक बचा हुआ अकाट्य और महान सत्य है। ऐतिहासिक भारतीय संकोच का जीता-जागता उदाहरण है। हम आक्रमणकारी नहीं हैं, हम हो नहीं सकते। हम अतिक्रमणकारी नहीं हैं, हम हो नहीं सकते। हम छीनते नहीं, क्योंकि छीन नहीं सकते। हम खुद को बदलते-बनाते चलते हैं। हम दूसरों की लकीर छोटी नहीं करते, अपनी छोटी ही सही, लेकिन जितनी भी लकीर है, उसे बचाते-बढ़ाते चलते हैं और चल रहे हैं। ठीक ऐसे ही चल रहा है श्रीमठ।
लोग कहते हैं कि मठों में बड़ा विलास और वैभव होता है, लेकिन सीधा-सादा श्रीमठ इस आधुनिक-प्रचारित तथ्य को सिरे से नकार देता है। श्रीमठ अपने भले होने की मौन गवाही देता है। अर्थात अपने होने में श्रीमठ ने उसी सज्जनता, सादगी और सीधेपन को बचाया है, जिसे आचार्य श्री रामानन्द जी ने बचाया था, जिसे कबीर ने पुष्ट किया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने घर-घर पहुंचा दिया।
यह परम सौभाग्य है कि आज श्रीमठ के पीठाधीश्वर जगदगुरु रामानन्दाचार्य स्वामी रामनरेशाचार्य जी भी सादगी के अतुलनीय प्रतिमान हैं। अपनी सम्पूर्ण सशक्त उपस्थिति के साथ वे इस कठिन काल में भी न्यायसिद्ध विद्वतापूर्ण सच्ची राम भक्ति के महान प्रमाण हैं। जैसे वे हैं, वैसा ही आज का श्रीमठ है, सीधा-सच्चा-सज्जन-बेलाग। आचार्य श्री में थोड़ी-सी भी असक्तता होती, तो श्री राम विरोधी विशालकाय भौतिक अभियान श्रीमठ को धकियाता-मिटाता समाप्त कर देता और बाकी बचे हुए को गंगा मैया की लहरें बहा ले जातीं। आज श्रीमठ खड़ा है, गंगा मैया को बताते हुए कि मां, मैं अब यहां से नहीं डिगने वाला। बनारस के गंगा तट पर वरुण घाट से अस्सी घाट तक इतना बेजोड़ राष्ट्र को सशक्त करने वाला दूसरा कोई मठ नहीं है।
यह बात सही है कि आक्रमण के कारण बीच में काफी लंबे समय तक श्रीमठ की गद्दी एक तरह से खाली हो गई थी। कोई रखवाला नहीं था, किन्तु रामभक्त वैष्णव सन्तों के आशीर्वाद और प्रेरणा से रामानन्दाचार्य श्री भगवदाचार्य जी ने श्रीमठ के नवोद्धार की नींव रखी। उनके उपरान्त रामानन्दाचार्य शिवरामाचार्य जी महाराज ने समृद्ध परंपरा की बागडोर रामानन्दाचार्य स्वामी रामनरेशाचार्य जी को थमा दी। आज श्रीमठ अपनी सुप्तावस्था से काफी आगे निकल आया है, जाति से परे जाकर सन्त सेवा जारी है, यहां से एक से एक विद्वान निकल रहे हैं, समाज, संस्कृति और संस्कृत की सेवा हो रही है। श्रीमठ आज हर पल जागृत है, आज उसकी पताका चहुंओर दृश्यमान होने लगी है। अब चिंता की कोई बात नहीं। आज वह जितना सशक्त है, उतना ही शालीन है। कोई शोर-शराबा नहीं, कोई ढोल-धमाका नहीं, केवल सेवाभाव, भक्तिभाव, रामभाव और सीताराम-सीताराम-सीताराम . . . .
सीतानाथ से प्रवर्तित वैदिक राममन्त्र एवं अनादि रामभक्ति धारा को मध्यकाल में (१४वीं-१५वीं शताब्दी) में परमसिद्ध, विलक्षण संगठनवादी, लोकोत्तर उदार, अदम्य उत्साही स्वामी रामानन्द जी ने अनुपम तीव्रता प्रदान किया, जिसके कारण देश के कोने-कोने में राम भक्ति की परम मंगलमयी धारा फैल गई। वर्तमान भौतिक विनाशक वातावरण के बावजूद रामानन्द सम्प्रदाय के आश्रमों, अनुयायियों, सन्तों एवं प्रचार का जोड़ किसी दूसरे सम्प्रदाय के साथ नहीं है। इस सम्प्रदाय से निकली हुई अनेक शााखायें आज लोक कल्याण योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जिनमें प्रमुख रूप से कबीर सम्प्रदाय, निराकारी सम्प्रदाय, रविदासी सम्प्रदाय, घीसापन्थी सम्प्रदाय, रामस्नेही सम्प्रदाय, गरीबदासी इत्यादि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। कुछ समानताओं को देखकर हिन्दी साहित्य के कुछ विद्वानों ने रामनुज सम्प्रदाय के अन्तर्गत ही रामानन्द सम्प्रदाय को स्वीकार किया है। आंशिक समानताओं के आधार पर तो सभी सम्प्रदायों को एकरूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। अलग-अलग मानने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी आंशिक साम्य के कारण किसी ने आद्य शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा था। उन्हें शंकराचार्य भी बौद्ध के रूप में दिखाई दिए, जिन्होंने बौद्धों के अवैदिक महल को भारत भूमि से उखाडऩे में अनुपम भूमिका निभायी। न्याय दर्शन के द्वितीय सूत्र – दुखजन्मप्रवृत्ति दोषिमिथ्या ज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्ग: के भाष्य की व्याख्या करते हुए वार्तिककार उद्योतकार ने सम्प्रदाय शब्द की व्याख्या में लिखा है शिष्याचार्यसम्बन्धस्याविच्छेदेन शास्त्रप्राप्ति सम्प्रदाय: – इसका भाव यह है – शास्त्र की वह प्राप्ति जो शिष्य एवं आचार्य के अविच्छिन्न सम्बन्ध के द्वारा हो, उसे ही सम्प्रदाय कहते हैं। स्वामी राघवानन्द जी ने स्वामी रामानन्द जी को राममन्त्र का उपदेश किया तथा रामोपासना में प्रवृत्त किया। जिसके आधार
पर सुनिश्चित होता है कि उन्हें भी अपनी अविच्छिन्न गुरु परम्परा से राम मन्त्र का उपदेश वैदिक सनातन धर्मोद्यान के परम संरक्षक स्वामी राघवानन्द जी कभी भी नहीं कर सकते थे। रामानुज सम्प्रदाय में कभी भी मुख्य रूप से राममन्त्र का उपदेश नहीं होता रहा है। श्री सीताराम कभी भी परमोपास्य के रूप में मान्य नहीं रहे हैं। अतएवं स्वामी राघवानन्द जी को या तो शास्त्र मर्यादा विमुख स्वच्छन्दचारी स्वीकार करना पड़ेगा या ऐसी वैदिक परम्परा में जोडऩा पड़ेगा, जिसमें राममन्त्र एवं रामोपासना का अनादि अविच्छिन्न प्रवाह हो। सभी सम्प्रदायाचार्यों ने अपने परमोपास्य को ही अपने सम्प्रदाय का मूल तथा परमाचार्य माना है। संन्यासी सम्प्रदाय भगवान शंकर को, रामानुज सम्प्रदाय भगवान लक्ष्मीनाथ इत्यादि। इसी क्रम से रामानन्द सम्प्रदाय का मूल एवं परमाचार्य किसी भी प्रकार से लक्ष्मीनाथ नहीं हो सकते। पूर्व लेखकों का लेखन ही जिनके लेखन का मूल आधार है, ऐसे वैदिक मर्यादाओं के ज्ञान से शून्य स्वतन्त्र चिंतन शक्ति से रहित भारतीय परम्पराओं के शत्रु एवं पाश्चात्य विचारों को ही परमवेद मानने वाले लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधकर रामानन्द सम्प्रदाय को रामानुज सम्प्रदाय के अन्तर्गत मान लिया। अन्य भी अनेक तर्क हैं, जिन्हें विस्तार के भय से उद्धृत नहीं किया जा रहा है। स्वामी भगवदाचार्य की जीवनी में इसकी विस्तृत चर्चा द्रष्टव्य है।
प्राय: परम्परा के सम्बन्ध में रामानुज सम्प्रदाय एवं रामानन्द सम्प्रदाय एक है या रामानुज सम्प्रदाय की शाखा रामानन्द सम्प्रदाय हैं, ऐसा बताने वाले लोग श्रीनाभा स्वामी जी के भक्तमाल के – रामानुज पद्धति प्रताप अवनि अमृत ह्वै अनुसर्यो – को उद्धृत किया करते हैं। इस छप्पय के पद्धति पद से स्वामी रामानन्द जी को रामानुज सम्प्रदायान्तर्गत सिद्ध करने का प्रयास किया करते हैं, किन्तु यहां जो पद्धति पद है, उससे सम्प्रदायानुयायी अर्थ करना नितान्त असंगत है। पद्धति शब्द सिद्धान्त का वाचक है न कि सम्प्रदाय का। स्वामी रामानन्द और स्वामी रामानुज के विशिष्टाद्वैत में बहुत कुछ साम्य भी है। दोनों आचार्यों को तत्वत्रय स्वीकृत हैं। अत: प्रतीत होता है कि कतिपय स्थानों पर सिद्धान्तत: दोनों के निकट होने के कारण पाठ भेद से रामानुज पद्धति पद का प्रचार हो गया। यद्यपि दोनों आचार्यों के इष्ट, मन्त्र उपासना पद्धति में भारी भेद है। भक्तमाल की कई प्रतियों में रामानन्द पद्धति का पाठ है। भक्तमाल में पद्धति शब्द सम्प्रदाय, पथ, मार्ग, परिपाटी के पर्यायवाची के रूप में आया है। छप्पय में रामानन्द पद्धति का प्रयोग प्रसंग को देखते हुए सर्वाधिक उपयुक्त लगता है। छप्पय में स्वामी जी की परम्परा का थोड़ा-सा वर्णन करके उनके यश का वर्णन हुआ है। अत: रामानन्द पद्धति प्रताप अवनि अमृत ह्वै अनुयर्यो (जिसका अर्थ हुआ – स्वामी रामानन्द जी का सिद्धान्त अमृत बनकर पृथ्वी पर फैला) सर्वथा प्रसंगानुकूल ही है।
पवित्र श्रीमठ में लगे इस चित्र में आपके बाएं से दाएं – जगदगुरु रामानन्दाचार्य जी महाराज, जगदगुरु रामानन्दाचार्य श्री भगवदाचार्य जी महाराज, जगदगुरु रामानन्दाचार्य श्री शिवरामाचार्य जी महाराज एवं वर्तमान पीठाधीश्वर जगदगुरु रामानन्दाचार्य स्वामी रामनरेशाचार्य जी महाराज।
श्री स्वामी भगवदाचार्य के अनुसार कुछ प्रतियों में रामानुज पद्धति पाठ भी है। जिसका अर्थ है – श्रीराम जी ही जिसके सर्वश्रेष्ठ उपास्य देवता हैं, ऐसी पद्धति का पृथ्वी पर प्रचार हुआ। इस पाठ (रामानुज पद्धति) और रामानन्द पद्धति में कोई सैद्धान्तिक विरोध नहीं है। स्वामी रामानन्दजी के सिद्धान्त से श्रीरामजी ही सर्वश्रेष्ठ उपास्य देव हैं। अत: रामानन्द पद्धति और रामानुज पद्धति, दोनों का एक ही भाव होने के कारण कोई विरोध नहीं है। इन तीनों पाठों में से किसी के द्वारा यह नहीं सिद्ध होता कि स्वामी रामानन्दाचार्य जी रामानुज सम्प्रदाय के दीक्षित शिष्य थे और रामानन्द सम्प्रदाय रामानुज सम्प्रदायान्तर्गत है।
शताब्दियों बाद श्रीमठ अपनी गौरवमयी आध्यात्मिक धारा की परिपुष्टि की दिशा में अग्रसर हो चला है। आचार्य प्रवर स्वामी रामानन्द जी ने अपनी परमोदात्त भावना से समाज के प्रत्येक वर्ग को श्रीराम भक्ति के परम मंगलमय महापथ पर चलाकर परमकल्याण से जोड़ते हुए देश को विखण्डन से बचाया था। श्रीमठ पथ विमुख समाज को अपने आदर्श एवं स्वरूप ज्ञान द्वारा पथारूढ़ करेगा। फलत: यह समाज और देश विखण्डन से बचेगा तथा अपनी शक्ति का उपयोग अपने अभ्युत्थान में करेगा। श्री सीतानाथ के चरणों में मेरी यही अभ्यर्थना एवं मंगल कामना है।
(जगदगुरु की कलम से)
श्रीमठ : हमारी आध्यात्मिक राजधानी
स्वामी जी के इन भावों को परिपुष्ट करती है भगवान श्रीकृष्ण की ये वाणियां –
तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च।
अन्तकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरम्।।
य: प्रयाति स सद्भावं याति नास्त्यत्र संषय:।।
हम जिसका पुन:-पुन: स्मरण करते हैं, उनमें ही हमारा प्रेम बढ़ता है। जब हम संसार का स्मरण करते हैं, तब हमारा प्रेम संसार में बढ़ता है। इसी क्रम में परमेश्वर का स्मरण उसमें प्रेम प्रकर्ष को उत्पन्न करता है, जो जीवन को कृतार्थ करता है। सुख सिन्धु का स्मरण ही सुखदाय हो सकता है, संसार का नहीं, क्योंकि वह तो दुखमय है, सुख रहित है। तभी तो गीता की सुस्पष्ट घोषणा है – अनित्यमसुखं लोकम् – अनित्य संसार नित्य सुखप्रद कैसे हो सकता है?
सगुण तथा निर्गुण रामभक्ति के माध्यम-गोमुख रामानन्दाचार्य की तप:स्थली एवं आध्यात्मिक राजधानी श्रीमठ भगवत् स्मरण का ही सर्वश्रेष्ठ स्मारक केन्द्र था। इसका पर उद्देश्य जन-जन में भगवत् स्मरण की गंगा को प्रवाहित करना था, जिसमें सभी संकुचित भेदभावों को छोडक़र लोग गोता लगावें एवं जीवन को परमोज्ज्वल बनावें। इस क्रम को अपूर्व सफलता मिली, जिसे आज भी रामभक्ति के विशालतम क्षेत्र एवं रामचरित्र के प्रति परम जनाकर्षण से मापा जा सकता है। श्रीमठ से प्रवाहित श्रीराम स्मारिका गंगा ने समाज के उन दरवाजों का भी स्पर्श किया तथा उनसे निकलने वाले लोगों को समान रीति से कृतार्थ किया, जिनकी छाया भी लोगों को अपवित्र बनाती थी। परमसन्त रविदास, संत शिरोमणि कबीर, धन्ना जाट एवं सेनानाई आदि इसके परम दृष्टान्त हैं। समाज के सभी वर्गों ने इससे शीतलता प्राप्त किया। एक दूसरे के बीच खाई मिट गई। विभिन्न तटों के बीच में सेतु का निर्माण हुआ। समाज विखण्डन की भयावह ज्वाला से बच गया। प्रत्येक के हृदय में दूसरों के प्रति सहानुभूति एवं स्नेह का उदय हुआ। इन व्यावहारिक लाभों से विशिष्ट होते हुए लोगों ने परम शान्ति को भी प्राप्त किया।
अनेक साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि श्रीमठ संसार के तत्कालीन आध्यात्मिक केन्द्रों में सर्वश्रेष्ठ था। भारत देश ही नहीं, संसार के सभी भागों से साधक एवं जिज्ञासु श्रीमठ में आते थे तथा पूर्णता को प्राप्त कर लौटते थे। इतिहासकारों का मानना है कि बारह प्रधान शिष्यों के अतिरिक्त स्वामी जी के पांच सौ विरक्त शिष्य थे, जो श्रीमठ में ही रहते थे। झोपड़ी से लेकर महल पर्यन्त के लोगों का आध्यात्मिक पिपासा की तृप्ति के लिए यहां आना-जाना था। तत्कालीन श्रीमठ की विशालता, भव्यता एवं जनाकर्षण के चश्मे से वर्तमान श्रीमठ को पहचानना उतना ही कठिन है, जितनी कठिनता सुदामा को अपनी झोपड़ी पहचानने में हुई थी। इसको देख श्रीमठ से प्रवाहित रामभक्तिगंगा के घाटों का आकलन करना किसी के लिए सम्भव नहीं है। पूरे देश में फैले श्रीमठ के अनुयायी आश्रमों तथा सन्तों की नामावली का संग्रह भी वर्तमान श्रीमठ में नहीं रखा जा सकता। यह दशा श्रीमठ की तब से हुई, जब औरंगजेब ने श्रीमठ का विध्वंस कर दिया। संसार का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक केन्द्र भयावह खण्डहर में बदल गया। राम-नाम संकीर्तन के बदले नमाज की धारा चल पड़ी। राम भक्तों की जमघट मौलवी-मुल्लों में बदल गई। दीर्घ काल तक रिक्तता एवं सूनापन की दशा बनी रही। लोगों ने धीरे-धीरे खण्डहर श्रीमठ की परिधि को घेरना शुरू किया। यह क्रम इतना प्रबल रहा कि श्रीमठ का सम्पूर्ण क्षेत्र घिर गया। आचार्य निष्ठा के क्षेत्र में कुम्भकर्ण तथा स्वकीर्ति मात्रैकशरण-साम्प्रदायिक-सिद्धान्तानभिज्ञ महन्तों, सन्तों एवं भक्तों की जब तक निद्रा खुली, तब तक उतना ही स्थान बच पाया था, जितना वर्तमान श्रीमठ का स्वरूप है। किसी विदेशी महिला अन्वेषक ने खोज किया है कि श्रीमठ की प्राचीन परिधि लगभग पांच किलोमीटर में थी।
संसार के सर्वश्रेष्ठ प्रकाशक को भी आज प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। यही तो श्रीराघव के संसार का वैचित्र्य है। वस्तुत: श्रीराघव ही शाश्वत, परम तथा निरपेक्ष प्रकाशक एवं स्मारक हैं तथा सर्वश्रेष्ठ स्मरणीय भी हैं। अपौरुषेय वेद की यही घोषणा है – तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। यही भाव हम सभी लोगों के संतोष का एकमात्र अवलम्ब है। श्रीमठ रामानन्द सम्प्रदाय का मूल एवं परम श्रद्धापरक पीठ है।
तुर्थ मंजिल पर रामजी के मंदिर के बाहर हॉल में महाराज के बैठने का स्थान झूला. यहाँ महाराज आगंतुकों से मिलते हैं.
श्रीमठ में विराजमान श्री हनुमनलला जी
गो माता को प्रणाम करते आचार्यश्रीगौशाला विहबंग दृस्य जो देखते ही बनता हैऔर गौशाला में आबल पूजन करते आचार्यश्री