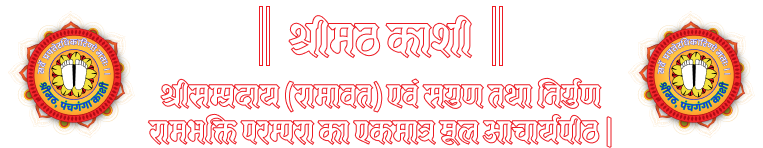डॉ. मारुति नन्दन तिवारी
काशी का पंचगंगाघाट मध्यकाल के महान वैष्णव सन्त एवं आचार्य रामानन्द जी का निवास स्थल था, जिसे आज ‘श्रीमठ’ के नाम से जाना जाता है । हिन्दू परम्परा में प्राचीन काल से ही पंचगंगाघाट का विशेष महत्त्व रहा है । काशी खण्ड के अनुसार पाँच पावन नदियों- गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा एवं धूतपापा का संगम स्थल होने के कारण ही इसे पंचगंगा घाट कहा गया है । यह घाट काशी के प्राचीनतम पक्के घाटों में है । इसका निर्माण लगभग १३वीं शती में राजस्थान के एक प्रसिद्ध राज्य आमेर के राजा मानसिंह ने कराया था, जिसका जीर्णोद्धार १६वीं शती में महारानी अहिल्याबाई द्वारा करवाया गया ।
काशी मुख्यतः शिव की नगरी मानी गयी है, जहाँ घाटों, गलियों एवं घरों में शिव के छोटे-बड़े आकार के असंख्य मन्दिर, शिवलिंग और प्रतिमायें देखी जा सकती हैं । भारतीय संस्कृति की समन्वयवादी प्रवृत्ति और देश की सांस्कृतिक राजधानी होने के कारण काशी में सर्वधर्म-समन्वय का भाव प्राचीन काल से ही देखा जा सकता है । यही कारण है कि शैव धर्म के साथ ही काशी में वैष्णव, शाक्त, सौर एवं बौद्ध तथा जैन धर्मों का भी पूरा प्रचार हुआ । बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली (सारनाथ) और जैन तीर्थकरों (सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ) की जन्मस्थली के रूप में बौद्ध एवं जैन परम्पराओं में काशी का महत्त्व सर्वविदित है । वैदिक परम्परा के सभी पाँच सम्प्रदायों (शैव, वैष्ण, शाक्त, सौर गाणपत्य) का काशी में महत्त्व रहा है काशी में शिव के लिंग एवं अन्य स्वरूपों के अतिरिक्त विष्णु के स्वतंत्र, विभव (अवतार) तथा चतुर्विंशति केशव, सूर्य के द्वादश आदित्य, शक्ति के विभिन्न शान्त एवं सहायक और नवदुर्गा तथा पंचगणेशों के पूजन की परम्परा साहित्य एवं पुरातात्विक अवशेषों दोनों से ही ज्ञात है ।
पंचगंगाघाट प्रारम्भ से ही काशी में वैष्णव सम्प्रदाय का केन्द्रीय स्थल रहा है, जिसे विष्णु काशी भी कहा गया है । मध्यकाल में गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी और मुगल शासकों के काल में उनकी धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता की नीतियों के कारण धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में एक गम्भीर संकट और चुनौती की स्थिति उत्पन्न हुई । ऐसी विकट परिस्थितियों में सामाजिक विचारकों एवं धर्माचार्यों की सदा से विशेष महत्वपूर्ण भूमिका रही है । मध्यकाल में भी समाज को दिशा देने और व्यवस्थित रखने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विचारकों एवं धर्माचार्यों ने अपनी-अपनी दृष्टि से कार्य किया ।
भारत की बहुदेववादी अनेकान्त चिन्तन परम्परा में वैदिककाल से ही ‘एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति’ का जो भाव स्वीकृत था, उसकी अभिव्यक्ति मध्यकाल में भी देखी जा सकती है । रामानन्द, कबीर, रैदास, गुरुनानक तथा ऐसे ही अनेक आचार्यों एवं विचारकों ने भारतीय परम्परा के समवेत स्वर को तत्कालीन आवश्यकता के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर पुनः अभिव्यक्त किया, मध्यकालीन धार्मिक आचार्यों में उत्तरभारत के वैष्णव आचार्य रामानन्द जी (१२९९ ई. से १४१०) का विशिष्ट और अग्रगामी स्थान है । सामान्य दृष्टि में विचार करने पर कुछ ऐसी बातें स्पष्ट होती हैं उच्च कुलीन ब्राह्मण, संस्कृत का मूर्धन्य पण्डित तथा प्रभावशाली वैष्णव सम्प्रदाय का आचार्य होने के बाद भी रामानन्द जी ने तत्कालीन सामाजिक स्थितियों और उनमें उपेक्षित परिवर्तनों के अनुरूप अपनी चिन्तन-धारा और कार्य-पद्धति को जिस कालसम्मत रूप में प्रस्तुत किया, उससे उनके स्वतंत्र निर्भीक, दूरदर्शी और देश हित को साध्य मानने वाले व्यक्तित्व की झलक मिलती है । तत्कालीन रूढ़िवादी पारम्परिक परिस्थितियों में इस प्रकार के परिवर्तन का उद्घोष धार्मिक क्षेत्र के लिए क्रान्तिकारी वैदिक धर्म में आये कालगत दोषों की दृष्टि से सामयिक था । ऐसी चुनौती को स्वीकारना रामानन्द जैसे साहसी और दृढ़ संकल्पी विचारक के लिए ही सम्भव था । मेरी दृष्टि में सामाजिक व्यवस्था के विकार, उन्हें दूर करने की तात्कालिक आवश्यकता और उसके प्रभावी उपायों के सम्बन्ध में जितनी गहरी सूझ रामानन्द में थी वैसी सम्भवतः दूसरे किसी मध्यकालीन धार्मिक आचार्य में नहीं दिखायी देती । रामानन्द की शुरूआत के बाद अनेक आचार्यों ने उनकी दृष्टि से कार्य किया, जिनमें कबीर, रैदास, गुरुनानक मुख्य हैं । यहाँ हम उनसे सम्बन्धित केवल तीन प्रमुख बिन्दुओं पर ही ध्यान केन्द्रित करेंगे ।
(१) विदेशी शासकों और उनकी कार्य पद्धति से तत्कालीन जातिगत दोषों एवं संस्कारों से दबी हुई व्यवस्था अपने पारम्परिक स्वरूप की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ हो रही थी । इस बात को रामानन्द जी ने भलीभाँति समझ लिया था, इसी कारण एक पारम्परिक और सम्प्रदाय विशेष का आचार्य होते हुए भी उन्होंने जातिगत असमानता की प्रवृत्ति को पूरी तरह तोड़ने का काम किया, जो समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ने के लिए प्राथमिक आवश्यकता थी । उन्होंने ब्राह्मण से अन्त्यज तक सभी जाति एवं वर्गों के लिए धर्म (भक्ति) का मार्ग प्रशस्त किया और इस प्रकार उन्हें चिन्तन की एक समवेत धारा से जोड़ा । स्वयं उनके शब्दों में-
‘जातिपांति पूछे नहि कोई, हरि को भजे सो हरि का होई’
(२) समाज के विचारक और धर्माचार्य की बातों सभी स्तर के लोगों तक पहुँच सकें, इसके लिए रामानन्द जी ने संस्कृत का प्रकाण्ड पण्डित होते हुए भी जनभाषा में अपनी बात कही जो उनके दूरदर्शी होने का प्रमाण है । तत्कालीन व्यवस्था में संस्कृत जनभाषा नहीं हो सकती थी, यह बात रामानन्द जी ने ठीक ढंग से समझी थी । यदि हम और पीछे के इतिहास को देखें तो बुद्ध और महावीर को भी जनभाषा में ही उपदेश देता हुआ पायेंगे । भ्रमण एवं उपदेश द्वारा जन सम्पर्क और अपनी बात के प्रचार की भारत में प्राचीन परम्परा रही है, जिसे राम के वनवास एवं बुद्ध तथा महावीर के अनवरत भ्रमण में देखा जा सकता है । रामानन्द जी ने भी विभिन्न स्थलों की यात्रा की थी और उपदेश दिया था देश और काल को सही सन्दर्भमें समझने के लिए यह नितान्त आवश्यक था ।
(३) मेरी दृष्टि में रामानन्द जी की सबसे महत्वपूर्ण और क्रान्तिकारी बात आराध्य देव के स्वरूप में परिवर्तन था । पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्यों के आराध्यदेव विष्णु और उनके लक्ष्मीनारायण स्वरूप रहे हैं, जबकि रामानन्द जी ने भारतीय जनमानस के मानसिक धरातल और संस्कारों से जुड़े एवं भारतीय परम्परा के आदर्श स्वरूप राम-सीता-लक्ष्मण को अपना आराध्य देव बनाया जो आगे चलकर रामानन्द जी द्वारा प्रवर्तित ‘श्री सम्प्रदाय’ के मुख्य आराध्य देव हुए । विष्णु एक पौराणिक चरित्र है, जबकि राम-सीता-लक्ष्मण भारतीय जनमानस से साधारणीकृत चरित्र रहे हैं, जिनमें मानव चरित्र के विभिन्न कोणों के आदर्श प्रतिमान देखे जा सकते हैं । व्यवहार और आचरण के स्तर पर उपासक राम-सीता-लक्ष्मण से जोप्रेरणा और आदर्श प्राप्त कर सकता था, वह विष्णु की उपासना से सम्भव नहीं था । इसी कारण रामानन्द जी ने इन्हें अपना आराध्य देव बनाया । तत्कालीन वियम परिस्थितियों में समाज के लिए ऐसे आदर्श चरित्र की नितान्त आवश्यकता थी ।
भारतीय परम्परा में जीवन में अनुकरणीय व्यवहारों की दृष्टि से इनसे श्रेष्ठ कोई अन्य चरित्र भारतीय देवमण्डल में नहीं है । अतः आराध्य देव के रूप में राम-सीता-लक्ष्मण की प्रतिष्ठा भारतीय समाज में आदर्श जीवन की प्रतिष्ठा थी ।
राम में लोकपरक आदर्श के सभी आयामों-पुत्र, भाई, पति, मित्र, पराक्रम, शासक, भक्ति का चरम बिन्दु देखा जा सकता है, शबरी के बेर खाने वाले, केवट राज को मित्र बनाने वाले तथा गिद्धराज जटायु का अन्तिम संस्कार करने वाले राम जैसे विशाल हृदय व्यक्तित्व को अपना आराध्य देव बनाकर रामानन्द जी ने समाज के समक्ष एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया था । दूसरी ओर लक्ष्मण और सीता भी विभिन्न वैयक्तिक आयामों में समाज के मान्य आदर्शों के प्रतिमान रहे हैं । इस दृष्टि से विष्णु के स्थान पर रामानन्द जी द्वारा आराध्य देव के रूप में राम-सीता और लक्ष्मण का प्रतिष्ठित किया जाना धार्मिक दृष्टि से कहीं अधिक सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था ।
उपर्युक्त क्रान्तिकारी परिवर्तनों के कारण स्वयं उनके अनुयायियों तथा अन्य सम्प्रदायों के आचार्यों में रामानन्द जी के प्रति विरोध का स्वर उठा होगा, किन्तु
उनके प्रासंगिक परिवर्तन का समाज के विशाल वर्ग ने पूरा समर्थन दिया होगा फलतः विरोध का स्वर शीघ्र ही मन्द पड़ गया होगा । यह रामानन्द जी का ही व्यक्तित्व था जिसने कबीर जैसे रूढ़िवादी धार्मिक परम्परा के प्रबल विरोधी व्यक्तित्व को न केवल अपनी ओर आकृष्ट किया बल्कि शिष्यत्व ग्रहण करने का संकल्प लेने को भी विवश किया । रामानन्द के १२ प्रमुख शिष्यों में जो नाम हमें मिलते हैं उनमें अधिकांश अलग-अलग जाति एवं वर्गों से सम्बन्धित थे । इनमें जुलाहे कबीर के अतिरिक्त चर्मकार रैदास, जाट कृषक धन्ना, नाई सेना, राजपूत राजा पीपा तथा भवानन्द, सुखानन्द, सुरसुरानन्द, अनन्तानन्द मुख्य हैं । रामानन्द ने स्त्रियों को भी जो सामाजिक व्यवस्था का आवश्यक अंग होती हैं परिवर्तन के लिए प्रेरित किया । इसी कारण उनकी शिष्य मण्डली में पद्मावती और सुरसरी जैसी स्त्रियों के भी नाम मिलते हैं । रामानन्द जी द्वारा प्रतिपादित पूर्ण समर्पित प्रपत्ति के भाव को अलग-अलग क्षेत्रों में आचार्यों एवं भक्तों द्वारा मान्यता मिली । रामानन्द जी के सामाजिक विचारों का प्रभाव कबीर एवं गुरुनानक पर तथा उनकी समर्पित भक्ति का प्रभावरैदास, रामानन्दाचार्य एवं तुलसी के काव्यों में मुखर हुआ ।
रामानन्द जी के मूल्यांकन में इतिहास-वेत्ताओं एवं साहित्यकारों को सर्वदा कठिनाई का अनुभव होता रहा है, क्योंकि उन पर विस्तृत सामग्री नहीं प्राप्त होती है । उनके दो प्रमुख ग्रन्थ श्री वैष्णवमताब्ज भास्कर एवं रामाचंनपद्धति हैं, जिनमें उनके दार्शनिक एवं वैष्णव भक्ति के विचारों का संकलन है, विद्वान् होते हुए भी पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थ लेखन से रामानन्द जी विरत रहे क्योंकि लेखन से अधिक महत्व उन्होंने अपने सिद्धान्तों के जनमानस में व्यावहारिक प्रचार को दिया ।
पंचगंगाघाट पर स्थित रामानन्द मठ आज ‘श्रीमठ’ के नाम से जाना जाता है । वर्तमान श्रीमठ का १९८३ ई. में अरविन्द भाई मफतलाल के प्रमुख सहयोगी द्वारा पूरी तरह जीर्णोद्धार कराया गया । फलतः सामान्य दर्शक के लिए श्रीमठ एक नवीन भवन है । रामानन्द पर विचार करते समय श्रीमठ की प्राचीनता पर विचार करना भी आवश्यक है । ध्यान से देखने पर श्रीमठ के नवीन भवन के निचले भाग (नींव) में प्राचीन भवन के कुछ अवशेष देखें जा सकते हैं । श्रीमठ के समीप पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर संवत् २०१६ (१९५९ ई.) और संवत् १८५७(१८०० ई.) के दो लेख मिले हैं । श्रीमठ के समीप ही माधव राज का धरहरा भी स्थित है, जिसे १७वीं शती ई. में औरंगजेब द्वारा मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया गया । समीप ही ग्वालियर के महाराज द्वारा १६वीं शती ई. में निर्मित कंगन वाली हवेली भी स्थित है । इस प्रकार श्रीमठ के समीपवर्ती भवनों एवं अन्य अवशोषों से १६वीं शती से निरन्तर इस स्थल पर होने वाले निर्माण कार्य की जानकारी मिलती है । स्वयं पंचगंगा घाट का निर्माण भी १३वीं शती ई. में राजस्थान के आमेर के राजा मानसिंह ने करवाया था । यह ऐतिहासिक तथ्य है कि रामानन्द जी ने पंचगंगा घाट पर रहकर अपने धार्मिक विचारों का प्रतिपादन किया था । अतः इस स्थान पर उनका मठ अवश्य रहा होगा । लेखक को आस-पास के क्षेत्रों के सर्वेक्षण के पश्चात् न केवल रामानन्द जी के मठ के १४वीं शती में इस स्थान पर विद्यमान होने का आभास हुआ, वरन् राम-सीता-लक्ष्मण की एक ऐसी प्रतिमा भी मिली जो ‘श्रीमठ’ की ऐतिहासिकता की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं । इस प्राचीन प्रतिमा के आधार पर रामानन्द जी द्वारा स्थापित मठ में उक्त प्रतिमा के प्रतिष्ठित और पूजित होने की सम्भावना व्यक्त की जा सकती है ।
राम-सीता-लक्ष्मण की यह प्रतिमा वर्तमान में कंगन वाली हवेली के राम मन्दिर में प्रतिष्ठित है । संवत् १६३९ (१५८२ ई.) के लेख से युक्त यह प्रतिमा
निश्चित ही रामानन्द जी द्वारा प्रतिपादित आराध्य देवों के स्वरूप के आधार पर निर्मित हुई है । रामानन्द जी के लगभग २०० वर्षों बाद बनी यह प्रतिमा श्री सम्प्रदाय में दो शताब्दी बाद भी रामानन्द जी द्वारा प्रतिपादित देवमूर्ति-स्वरूप के पूजन की परम्परा को प्रकट करती है । रामानन्द जी की अवधारणा के अनुरूप ही यह प्रतिमा आकार में भी छोटी (लगभग २ ऊँची) है । यह प्रतिमा निश्चित ही तत्कालीन रामानन्द सम्प्रदाय के ‘श्रीमठ’ में प्रतिष्ठित रही होगी । जो बाद में औरंगजेब या अन्य किसी परवर्ती मुगल शासक के समय हिन्दू धर्म और उनसे सम्बन्धित मठ-मन्दिरों को पहुँचाये गये क्षति के फलस्वरूप रामानन्द सम्प्रदाय के किसी भक्त द्वारा कंगन वाली हवेली में प्रतिष्ठित की गयी क्योंकि रामानन्द मठ मुसलमान शासकों द्वारा पूरी तरह क्षतिग्रस्त किया जा चुका था । रामानन्द जी के सामाजिक और घार्मिक परिवर्तन के उदारवादी समन्वयात्मक विचारों के कारण समाज में उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए मुसलमान शासकों ने निश्चित ही रामानन्द मठ को क्षति पहुँचायी होगी । यही कारण है कि श्रीमठ (रामानन्दाचार्यपीठ) हमें मूलरूप में नहीं प्राप्त होता है ।
रामानन्द ने सीता और लक्ष्मण सहित श्रीराम के ध्यान का प्रतिपादन किया है । इसीलिए रामानन्द सम्प्रदाय से सम्बन्धित प्राचीन मन्दिरों में ऐसी विभूति की प्रतिष्ठा एवं पूजन की परम्परा मिलती है । सीता और लक्ष्मण सहित राम की मूर्ति का सुन्दर ध्यान-मन्त्र रामानन्द कृत श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर में भी मिलता है-
विकचपद्मदलायतवीक्षणं, विधिभवादिमनोहरसुस्मितम् ।
जनकजादृगयाङ्गसमीक्षितं,
प्रणतसत्समनुग्रहकारिणम् । । ५५ । ।
मुनिमनः सुमधुव्रतचुम्बितस्फुटलसन्मकरन्दपदाम्बुजम् ।
बलवदद्भुतदिव्यधनुःशरा महितजानुविलम्बिमहाभुजम् । । ५६ । । परार्ध्यहाराङ्गदचारुनूपुरंसुपद्मकिंजल्क पिसङ्गवाससम् ।
लसद्घनश्यामतनुं गुणाकरं कृपार्णवं सद्धदयाम्बुजासनम् । ।५७ । । प्रसन्नलावण्यसुभृन्मुरवाम्बुजं नरं शरण्यंशरणं नरोत्तमम् ।
सहानुजं दाशरथिं महोत्सवं स्मरामि रामं सह सीतया सदा । । ५८ । । रामानन्द जी के आराध्य देव राम मनोहर छबि वाले, प्रसन्न वदन एवं अलंकरणों से सज्जित तथा धनुष और बाण से सुशोभित होंगे । राम के दक्षिण पार्श्व में लक्ष्मण और वाम पार्श्व में सीता निरूपित होंगी । कंगन वाली हवेली की १५८२ ई. की मूर्ति में रामानन्द जी के ध्यान के अनुरूप ही धनुष-बाणधारी राम को लक्ष्मण
और सीता सहित दिखलाया गया है । समभंग में खड़े राम के दक्षिम पार्श्व में धनुष एवं बाण से युक्त लक्ष्मण एवं वाम पार्श्व में जलपात्र एवं पद्म से युक्त सीता की स्थानक (आकृतियाँ) बनी हैं । काले पत्थर में उकेरी इस मूर्ति में राम के साथ किरीट, मुकुट एवं अन्य अलंकरण द्रष्टव्य है । राम और लक्ष्मण दोनों के ही पीठ पर तूणीर देखा जा सकता हैं वर्तमान में श्री मठ में प्रतिष्ठित आराध्यकी त्रिमूर्ति पूर्णतः उपर्युक्त प्रतिमा के समान है ।
यद्यपि काशी के विभिन्न क्षेत्रों में कुषाण काल (दूसरी शती ई.) से १९वीं शती ई. के मध्य की विभिन्न धर्मों से सम्बन्धित आराध्य देवों की अलग-अलग स्वरूपों वाली प्रभूत मूर्तियाँ मिली हैं । किन्तु राम-सीता-लक्ष्मण के उपर्युक्त मूर्ति के पूर्व की कोई भी ऐसी त्रयी प्रतिमा काशी से नहीं मिली है । जिससे स्पष्ट है कि राम-सीता-लक्ष्मण की त्रयी मूर्ति के निर्माण की परम्परा रामानन्द से पूर्व काशी में लोकप्रिय नहीं थी । अतः उपर्युक्त मूर्ति १६वीं शती में पंचगंगा घाट पर रामानन्द सम्प्रदाय की विद्यमानता प्रभावित करती है और साथ ही यह भी संकेत देती है कि रामानन्द सम्प्रदाय के श्रीमठ में यह मूर्ति उपास्य प्रतिभा के रूप में प्रतिष्ठित रही होगी । १६वीं शती में उपर्युक्त मूर्ति के निर्माण से उस काल में रामानन्द मठ के पंचगंगा घाट पर स्थित होने का निश्चित प्रमाण मिलता है जिसे बाद में किसी समय मुसलमान शासकों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया । इस प्रकार श्रीमठ वर्तमान नवीन स्वरूप वस्तुतः पूर्व में बने प्राचीन मठ का ही पुर्ननिर्माण किया ।
वर्तमान श्रीमठ में रामानन्दजी की चरण पादुका एवं उनकी ध्यानस्थ मूर्ति के अतिरिक्त तुलसी और कबीर की भी मूर्तियाँ स्थापित हैं । वर्ष १९८३ में निर्मित इन मूर्तियों में रामानन्द की ध्यानस्थ मूर्ति में ललाट एवं शरीर के अन्य १२ भागों पर ऊर्ध्वपुण्ड्र देखा जा सकता है । उनका बायां हाथ घुटनों पर स्थित है । रामानन्द जी मुण्डित मस्तक प्रभामंडल से युक्त है । बायी ओर व्याख्यान मुद्रा में दोनों पैर मोड़कर विराजमान कबीर की मूर्ति है, जबकि दाहिनी ओर ग्रन्थ (रामचरितमानस) एवं तुलसी माला से युक्त तुलसीदास की आसन मूर्ति बनी है ।
श्रीमठ प्रकाश/४१